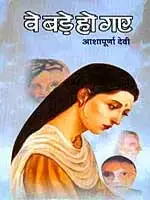|
नारी विमर्श >> वे बड़े हो गए वे बड़े हो गएआशापूर्णा देवी
|
|
|||||||
प्रस्तुत है उत्कृष्ठ उपन्यास...
15
तीनों बहनें एक कमरे में सोती हैं, देर रात तक गप्पें लड़ाती हैं । सुलेखा भंडारवाले कमरे से सुन नहीं पाती। आज बरामदे में बैठी है, तभी.. .
अचानक वह अपने बच्चों की आवाज नहीं पहचान पाती है, किसकी आवाज है यह?
"रहने दे वह सब बड़ी-बड़ी बात; जरा सोच तो, बैठक में एक सोफा सेट तक नहीं है। इस युग के किसी सभ्य परिवार में कोई घूमने आए तो वही दो विशाल हैंडलवाली और दो लोहे की कुरसियाँ । जगह नहीं बनती तो बैठ जाओ बिस्तर पर। यह सबकुछ ही तो पैसे की कमी के कारण नहीं है?"
"पता है, दीदी। रूबी की माँ को घर सजाने का इतना शौक है कि मिट्टी की मामूली सुराही खरीदकर उसपर पेंटिंग करती है और हरे पत्तों की झाड़ी लगाकर कमरे के कोने में सजाकर रखती है। इसमें तो खास खर्चा भी नहीं होता।"
"तभी तो कहती हूँ रे, पैसा ही मूल कारण नहीं है। मूल बात है रुचि। रुचि की कमी के कारण ही यह हाल है हम लोगों का। इस घर को चमकाकर आधुनिक बना डालना असंभव है।"
तिन्नी की ही-ही सुनाई पड़ती है, “अर्थात् जिस तरह बुड्ढी पर पेंट चढ़ाकर उसे तरुणी बनाना संभव नहीं है!"
"तू तो बड़ी मसखरेवाली हो गई है आजकल! हाँ, मगर कहा ठीक ही। घर में कदम रखते ही आँखों को चुभने लगती है उस बुढ़ापे की छाप । बाबूजी की बैठक के दरवाजे पर टँगा परदा है, क्या परदा है? पुरानी चादर का एक पगड़ा हुआ टुकड़ा। सीढ़ी के सामने ही बड़े-बड़े पैकिंग बॉक्स में रखा है कोयले का ढेर और थोड़ा आगे बढ़ते ही."
अचानक नीरा की आवाज रेडियो की कमेंट्री की तरह बुलंद हो उठी, "वहाँ देखिए, उस टोकरी में पड़े हैं लकड़ी की गोइठ आदि जलावन के ढेर । आगे बढ़िए, जीने पर से आगे बढ़ते जाइए। क्या देख रहे हैं आप? गंदे कपड़े रखने का बक्सा है न! मगर उस बक्से पर ढक्कन है क्या, नहीं। क्योंकि यह पुरखों के जमाने का है। कभी किसी युग में एक दिन उसका ढक्कन गायब हो गया। अत: अब वह गधे की पीठ का मौसेरा भाई बन गया है।"
तीनों बहनों के हँसकर लोट-पोट होने की आवाज आती है।
फिर भी नीरा रुकती नहीं है। उसी ढंग से वर्णन करती जाती है, "सीढ़ी पर चढ़ते ही कितने प्यार से लड़खड़ाते हुए दो स्टूल पर सुराही में पानी रखा है, खाने की मेज के नाम पर जो बिछी हुई है, दरअसल वह घर की गृहिणी के दादा ससुर के लिखने की मेज थी। उस जमाने का था, इसलिए इतना विशाल। उसी से काम चलाया जा रहा है और बड़े जोश से उसे डाइनिंग टेबल का दरजा दिया जा रहा है।"
नीरा के कहने के ढंग में कौतुक भरा है। उसकी कमेंट्री सुनकर बाकी दोनों बहनें हँसकर लोट-पोट होती हैं।
सुलेखा धीरे-धीरे हँसुए और टोकरी को उठाकर भीतर चली आती है। उसे डर लगता है कि हँसकर लोट-पोट होते-होते अचानक अगर वे बरामदे में न आ जाएँ।
क्या सुलेखा उतने थोड़े समय में गाल पर बह गए इतने सारे आँसू पोंछ पाएगी?
वे तो सपने में भी इसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे, इसमें क्या शक है? मजाक ही तो कर रहे हैं वे।
अत: माँ के इस विचित्र आचरण का कोई अर्थ उनकी समझ में नहीं आएगा।
क्या सुलेखा के मन की गहराई में तसवीर की तरह सजी-सँवरी एक गृहस्थी का सपना नहीं था? मगर अभिमानी सुलेखा उसके लिए हाय-तौबा, जो नहीं है या जो नहीं हो सकता, नहीं मचा सकती है। जितना है, उसी में मैं संतुष्ट हूँ। इसी धारणा में उसे सम्मान दिखाई पड़ता है।
सब्जी रखकर सुलेखा छोटी सी खिड़की के पास जाकर खड़ी थी। पीछे से निशीथ की दबी आवाज गरज उठी, "रात के बारह बजे तक कौन से भोज की तैयारी हो रही है?"
सुलेखा के गालों पर आँसू अब सूख चुके थे। इसीलिए जल्दी से पलटकर सहज भाव से बोली, "होगा क्या? यही सवेरे की थोड़ी-बहुत तैयारी कर रही थी।"
"घर में कल कोई होम-यज्ञ है क्या?" निशीथ के स्वर में व्यंग्य था।
हमेशा से ही परिस्थिति को हलका बनाने के लिए सुलेखा ऐसे सहज भाव से बात करती है। उसी हलके स्वर में बोली, "यज्ञ तो रोज ही है। मसूर की दाल, कटहल की तरकारी, पकौड़े, बैंगन-करेला और मछली की रसेदार तरकारी-यही यज्ञ है।"
लौटते हुए नाराज स्वर में निशीथ कह गया, "उसी की तैयारी में रात के बारह बज जाते हैं। सूरज की रोशनी में जो काम बिना खर्च के हो सकता है, उसके लिए घंटों बिजली खर्च की जाती है।"
खैर, सुलेखा समझती है, वह बिजली के खर्चेवाली बात निशीथ ने जानकर जोड़ दी है। अभी तक कमरे में नहीं गई, इसलिए निशीथ को अच्छा नहीं लग रहा है। दिमाग का पारा गरम हो रहा है। कहीं यह बात सुलेखा के सामने भी न खुल जाए, इसीलिए इस बात का संयोजन किया गया। प्रेस्टीज के मामले में बहुत ही सचेतन है निशीथ। और उसके चरित्र से तो सुलेखा भलीभाँति परिचित है। अच्छी तरह जानती है कि कहाँ उसकी कमजोरी है
और किस बात से उसका अहम् जुड़ा है। सब जान चुकी है, फिर भी कभी उसे पूरी तरह मुट्ठी में भरने की कोशिश नहीं की, डरती ही रही।
किसी जमाने में सुलेखा की पराश्रिता माँ सुलेखा को सीख देती थी कि दुनिया में जोर दिखाकर जीतने की कोशिश मत करना, बेटी। उससे तुम छोटी ही हो जाओगी । जान लो, भय से ही जय है। लोगों को तुम मानकर चलोगी तो लोग भी तुम्हें मानकर चलने के लिए बाध्य होंगे।
माँ के उपदेश को 'सिर-आँखों पर' रखकर चलती आई है सुलेखा, मगर लाभ क्या हुआ? आशानुरूप फल मिला क्या? तो क्या सुलेखा यही समझ ले कि उस जमाने की थ्योरी इस जमाने में नहीं चलती है? फिर भी सुलेखा गृहस्थी की चक्की घुमाए चली जा रही है, घुमाए जा रही है सिलाई मशीन का चक्का भी। और जैसे ही कपड़ों का ढेर सिल जाता है, बंडल बनाकर समिति के ऑफिस में पहुँचाने चल देती है।
|
|||||


 i
i