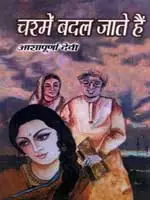|
नई पुस्तकें >> चश्में बदल जाते हैं चश्में बदल जाते हैंआशापूर्णा देवी
|
|
|||||||
बाप बेटा को समझाना चाहता है कि युग बदल गया है-तुम्हारा चश्मा बदलना जरूरी है। वृद्ध पिता के चेहरे पर हँसी बिखर जाती है।
4
उसके चले जाते ही सोमप्रकाश हिलते हुए पर्दे की तरफ देखने लगे। एक शिशु एक खस्ताहाल होते जीवन में कितनी जीवनीरस भर सकता है? ये छोटा-सा शिशु अगर सोमप्रकाश के कब्जे में होता, अगर सोमप्रकाश उसके कोमल शरीर और कोमल फूल से हृदय का स्पर्श कर सकते तो शायद पृथ्वी के मामले में इतने निर्मोह न हो जाते।
अचानक कब किस ज़माने में पाठ्यपुस्तक में पढ़ी एक कविता की दो लाइनें याद आ गईं-'छोटे छोटे छोटे नन्दन जिसके घर, नन्दन वन में वही तो बस्ती बनाता है...'
हालाँकि पहले ये बात सस्ते किस्म की सेन्टीमेन्टल बात लगती थी पर आज सहसा लगा या महसूस हुआ, इस बात में एक उपलब्धि की बात छिपी है। और इसी के साथ लगा कि पहले ज़माने के बड़े-बड़े सम्मिलित परिवारों के बुजुर्ग लोग कितने सुखी होते थे। दिन-रात उनके आसपास-इसी तरह के छोटे-छोटे इन्सानों का मेला लगा रहता था। वे लोग 'ताऊजी' से 'दादा' और फिर 'बूढ़े दादाजी' में तब्दील होकर प्रो-नाती-पोतों के संग का मजा उठाते थे। उपभोग करते थे।
उपभोग?
हाँ उपभोग ही तो। जैसे इन्सान प्रकृति की श्यामालिका उपभोग करता है।...'हरा' ही तो 'प्राणरस' है। हरियाली ही तो आँखों को सुख और मन को परितृप्त करती है।
तब-वही तब के बूढ़े क्या आज जैसे अधिकारविहीन दरिद्रों की भूमिका अदा करते थे?
वे लोग ही तो थे अथाह सम्पत्ति समूह के मालिक।...बच्चों के माँ-बाप? उनकी भूमिका तो साइड की भूमिका थी।
बच्चे भी यही जानते थे, तभी तो वे लोग मातृदेवी के भौंहे सिकोड़कर अनुशासन क्रिया से छिटक कर भाग आते थे और आकर अनायास ही दादा-दादी के पास आकर माँ-बाप की निन्दा करते थे। बेझिझक माँ-बाप को धमकाते थे-'ईश! मुझे मारा? अभी दादी से बता देता हूँ।' 'दादाजी देखो; पिताजी पढ़ाने क्या बैठे है, बार-बार मेरा कान खींच रहे हैं। मैं अबसे पिताजी के पास नहीं पढ़ूँगा-तुमसे पढ़ूँगा।'
तो क्या वे माँ-बाप सोचते थे कि उनका सम्मान घट रहा है? वे सोचा करते थे कि उनकी सम्पत्ति पर दूसरे कब्जा कर उन्हें वंचित कर रहे हैं? या 'अपनी सम्पत्ति पर पूरी तरह से हक़ बनाए रखने के लिए विपक्ष को पास ही भटकने न देने में ही बुद्धिमानी है।'
उस समय दादा-दादी द्वारा पाले गये शिशु क्या 'अमानुष' या निकम्मे होते थे? पुरातन युग के मनीषीगणों की तालिका क्या यही सिद्ध करती है?
कैसे आश्चर्यजनक ढंग से बदल गया इस नितान्त साधारण बंगाली समाज का मानचित्र?
अब? अब 'शिशु' नामक विराट सम्पत्ति, जो 'समाज का भविष्य' है या फिर 'भविष्य का समाज' है, केवल एक ही मालिक के कब्जे में है। मालिक भी कहना उचित न होगा, अब है 'मालकिन'-उन्हीं का एकछत्र अधिकार है।
वे ही इस 'शिशु' नामक देवदूत को अपनी मुट्ठी में बन्द रखकर सिर्फ अपने ही ढंग से ढालने के लिए दृढ़-संकल्प हैं।...अगर उसकी इच्छा हो तो उससे 'चूहादौड़' करवाकर उसके 'शैशव' नामक अमूल्य सम्पदा को कुचलकर नष्ट कर सकती है। और अगर चाहा तो उसको 'आने' ही नहीं दिया। वंचित ही रखा शिशु को दुनिया की रौशनी से।
यह युग उनके पक्ष में है।
कानून उनका सहाय है।
आधुनिक समाज उनका समर्थक है।
सोमप्रकाश के घर में भी तो 'शिशु' की कमी होने की कोई वजह नहीं है। उनके बड़े बेटे की शादी को आठ साल हो चुके हैं।
छोटे की शादी हुए छह साल हो गये हैं।
उस समय के 'स्वाभाविक नियम' से चले होते तो सात-आठ पैदा कर ही सकते थे। लेकिन न कर सके।'
बड़े बेटे की केस हिस्ट्री ये है कि शादी के साल भर के अन्दर ही, गलती से असतर्कतावश, एक घटना घटित होने की आशंका से, अस्थिर भाव से भागदौड़ करके विपन्न अवस्था से मुक्त होने गये तो ऐसी कोई गड़बड़ी हो गई कि अब शायद उस अवस्था से कभी भी उद्धार न हो सकेगा। शायद आगे चलकर बड़ी बहू की भूमिका 'निःसन्तान' की ही रह जाए।
लेकिन-अब तो लगातार 'विज्ञान' बहुत कुछ आश्वासन दिए जा रहा है इसलिए हो सकता है बंजर पड़ी ज़मीन में भी फसल उगाई जा सके।
मानों सब-कुछ हाथ की मुट्ठी में है। इसीलिए अब 'पाना-न-पाना' नहीं 'लेना-न-लेना'।
और छोटे लड़के के यहाँ, कौन जाने निजस्व इच्छा से अथवा अचानक असतर्कतावश, इस देवदूत का आविर्भाव शादी के दो साल बाद हुआ है।
पर बहू दूसरों से सुना-सुनाकर बताती है-'बाबा, सासुमाँ 'पोता' 'पोता' 'वंशधर' 'वंशधर' कहकर इस क़दर पगलाई थीं कि मजबूर होकर आनन-फानन पैरों में जंजीर पहनना पड़ा।'
जबकि आश्चर्य की बात तो ये है कि उसी जंजीर को ऐसा जकड़ कर सँभालकर रख दिया है कि दूसरा कोई ज़रा हिला-डुलाकर देखना चाहे तो देख नहीं सकता है।
अधिकार प्रकाश की तीव्रता कितनी प्रखर है और कितना निर्लज्ज हुआ जा सकता है यह देखना हो तो इन 'हाल ही में हुई जननियों' को देखो। शिशु नामक दुर्लभ वस्तु केवल अपना है, इस परम सत्य को बाक़ी सारे लोगों को उठते-बैठते जताकर मानती हैं।
यहाँ तक कि उस सम्पत्ति का प्रधान हिस्सेदार की भूमिका भी अनाधिकारी की ही है।
ऐसा क्या सोमप्रकाश के घर में है?
नहीं-नहीं। घर-घर यही दृश्य है।
अगर अपने प्रयोजन पर दया करके कुछ देर के लिए बच्चे को उसके दादा-दादी के जिम्मे कर जाती है तो इसी से वे कृतार्थ हो जाते हैं। और महिला के वापस लौटते ही बच्चे के असीमित गुणों और बुद्धिमता का उदाहरण सुनाते-सुनाते प्रशंसा के पुल बाँध देते हैं। यह भी एक तरह की खुशामद ही है। इसके अलावा अगर गलती से उनके मुँह से निकल जाए कि अभी तक वे लोग कितना परेशान हुए है या बच्चे ने कितना तंग किया है तो भविष्य में फिर कभी क्या वह सौभाग्य प्राप्त होगा?
ये ही है आजकल के बूड्ढे-बूढियों का जीवन-चित्र।
अच्छा क्या सोमप्रकाश शैशवकाल में अपनी दादी से डाँट नहीं खाते थे? ओ बाबा। 'दादी' को जितना चाहते थे उतना ही डरते थे।...घर में ढेर सारे चचेरे भाई-बहनों के साथ दौड़-धूप करते वक्त अगर कोई 'दुष्कर्म' हो गया और दादी ने अन्तराल से ही पूछ लिया-'कौन है रे वहाँ? कौन कमरों को तहस-नहस कर रहा है? क्या घर तोड़ डालोगे तुमलोग?'
बस! पलभर में जादू की तरह खामोशी छा जाती। और दादाजी के पास? 'सुलेख' ज़रा भी खराब होता तो कान पकड़कर एक पाँव पर घंटों खड़ा नहीं होना पड़ता था? सोमप्रकाश के दादाजी पोते-पोतियों के सुलेख पर पैनी नज़र रखते थे। उनका मानना था कि अगर मामूली से अक्षरों को सुन्दर ढंग से लिखना नहीं सीखेंगे तो जीवन को सुन्दर बनाना कैसे सीख पाएँगे?
हालाँकि चाचालोग पीठ पीछे कहते थे-'पिताजी भी हद करते हैं। किस से किस की तुलना?'
पर वही पीठ पीछे। सामने कोई बहस नहीं करता था कि-'यह तुम्हारी सनक है पिताजी। एबसर्ड तुलना।'
|
|||||


 i
i