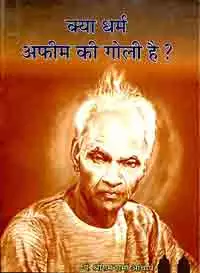|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> क्या धर्म अफीम की गोली है ? क्या धर्म अफीम की गोली है ?श्रीराम शर्मा आचार्य
|
|
||||||
क्या धर्म अफीम की गोली है ?
विज्ञान उपयोगी है, परिपूर्ण नहीं
विश्व में फैली ज्ञान की दो धाराओं धर्म और विज्ञान का प्रादुर्भाव दो भूमिखंडों से हुआ है। समस्त जीवित और महान धर्मों की जन्मभूमि आज का सीमित, किंतु कभी का बृहत्तर भारत है। प्राकृतिक विज्ञानों का पाश्चात्य जगत। एक अंतर्मुखी और आत्मनिष्ठ है, दूसरा बहिर्मुखी और वस्तुनिष्ठ। एक इंद्रियातीत तत्त्वों के रहस्यों के उद्घाटन में व्यस्त, दूसरा इंद्रियग्राह्य वस्तुओं के संदर्भ में प्रयत्नशील।
भारतीय विचारधारा मूलतः धार्मिक विचारधारा है। हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी, मुसलमान और येरुशलम की भूमि में उपजे क्रिश्चियन धर्म की रोमन कैथोलिक शाखा का अनुयायी ईसाई-इन सबकी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन जीने की रीति-नीतियाँ, मान्यताएँ, दृष्टिकोण और व्यावहारिक गतिविधियाँ अपने-अपने धर्मों के द्वारा प्रतिपादित नियमों द्वारा नियमित और संचालित होती हैं, किसी समय आध्यात्मिकता उत्पन्न करने वाला यह सारा क्षेत्र बृहत्तर भारत की परिधि में आता था, जिसे इन दिनों एशिया कहते हैं।
देश, काल, परिस्थिति ने इन धर्मों को भिन्न-भिन्न कलेवर तो धारण करा दिए हैं, कर्मकांड और विचार-व्यवहार के ढंग तो अलगअलग कर दिए हैं, परंतु उनका मांस और प्राण, उनकी मूल मान्यताएँ बहुत बड़े अंश में समान हैं। उदाहरणार्थ उपरोक्त सभी धर्म मरणधर्मा शरीर को नियंत्रित और संचालित करने वाली ऐसी सत्ता-आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जिसका इस जीवन के परे भी अस्तित्व बना रहता है। तथा ऐसी ही अन्य उभयनिष्ठ आधारभूत मान्यताओं ने इन धर्मों के अनुयायियों के संपूर्ण जीवन को, इंद्रिय-मस्तिष्क, हृदय की प्रत्येक क्रिया को, अनुशासित करने का न केवल प्रयत्न किया है, वरन् परलोक के लोभ और भय दिलाकर आत्मा के कल्याण के लिए अनेक विधि-निषेधों को मानने को मजबूर भी किया है।
इसे स्वस्थ्य स्थिति नहीं कहा जा सकता। एशियायी धर्मों ने स्वर्ग और निर्वाण के प्रति, पारलौकिक जीवन के प्रति, अपने अनुयायियों के झुकाव, रुचि और ललक को इतना तीव्र कर दिया है कि इहलोक का मूल्य भव-बंधन एवं माया जाल कहा जाने लगा। वैयक्तिक जीवन से श्रम, कर्म, स्वावलंबन और आत्मविश्वास, पारिवारिक जीवन से घनिष्ठता-उदारता तथा सामाजिक जीवन में सामूहिकता की भावना और सहयोग जैसे सद्गुण इस पारलौकिकता की अति से लुप्त होने लगे। अपनी मेहनत से धरती को स्वर्ग बनाने और इसी जीवन में स्वर्ग में रहने का आनंद पाने के बदले किसी बने बनाए स्वर्ग में मृत्यु के उपरांत पहुँचने और सुख पाने की मोहक कल्पना ने जन मानस को ग्रस लिया। परलोकवाद का एकांगी पक्ष एक घातक रोग बन गया और उसने सर्वतोमुखी प्रगति के मार्ग में बाधा ही पहुँचाई।
इसके विपरीत पश्चिमी विचारधारा मूलतः विज्ञान प्रेरित विचारधारा है। इंद्रियग्राह्य वस्तु व विषय ही प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन एवं अनुसंधान का क्षेत्र है। अब तक के अधिकांश वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य केवल इतना रहा है कि ऐहिक जीवन को अधिक सुख-सुविधा युक्त बनाने के लिए प्रकृति का दोहन किस प्रकार किया जा सकता है? इस विचारधारा ने जहाँ मनुष्य को साहसी, कर्तव्यपरायण, कर्मशील और व्यावहारिक बनाया है, वहीं उसे बहिर्मुखी, सुखवादी और अनात्मवादी भी बना दिया है। कर्मफल के नियम और आत्मकल्याण की कल्याणकारी आस्था को हटाकर, औचित्य की समस्त सीमाओं को लाँघती विलासिता ने तथा स्नेह रहितता, असुरक्षा और तनाव ने पश्चिमी मन को ग्रस लिया।
यद्यपि यह सही है कि धर्म के समान प्राकृतिक विज्ञान भी गणित की गिनती, भौतिकी की ऊर्जा, रसायन की संयोजकता जैसे अनेक अवस्तुनिष्ठ विचारों (ऐब्सट्रेक्ट आइडियाज) की नींव पर टिके हैं, तथापि यह भी सही है कि उन विज्ञानों से उपजी पश्चिमी विचारधारा व सभ्यता का वर्तमान स्वरूप केवल वस्तुनिष्ठता या वैषयिकता से, अर्थात केवल इहलोकवाद से नाता जोड़े हुए है। परलोकवाद के समान इहलोकवाद भी पश्चिम का एक संक्रामक घातक रोग बन चुका है।
धर्म और विज्ञान की ये स्थितियाँ एक दूसरे के बिलकुल विरुद्ध पड़ती हैं और प्रतीत होता है कि उनमें समझौते की तनिक भी संभावना नहीं है, किंतु सूक्ष्म विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली विचारधाराओं के बीच में संतुलन का बिंदु भी विद्यमान है। गतिमान पेंडुलम जब बाएँ या दाएँ छोर पर पहुँच जाता है, तब विपरीत दिशा में लौटने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता। यह डोलना, यह अस्थिरता उस समय तक जारी रहती है, जब तक कि मध्य की संतुलित स्थिति स्थाई रूप से प्राप्त न हो जाए। आत्मवादी धर्म और पदार्थवादी विज्ञान को मध्यमान संतुलन-बिंदु की विपरीत दिशाओं में स्थित जो अतिवादी व अस्थाई स्थितियाँ हैं, वहाँ से उन्हें संतुलन बिंदु की ओर लौटना ही होगा। इससे मिलता-जुलता उदाहरण देते हुए हरबर्ट स्पेन्सर यह मत प्रतिपादित करते हैं कि अंतिम सीमा तक विकसित हुए भावनात्मक (धार्मिक) संस्कृति को चेतनात्मक (पदार्थवादी) संस्कृति की दिशा में तथा चेतनात्मक संस्कृति को भावनात्मक संस्कृति की दिशा में लौटने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार इस विचित्रकिंतु तर्कसिद्ध निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि परम सत्य की खोज में संलग्न धर्म और प्राकृतिक विज्ञान अस्थाई स्थितियों पर स्थित होने के कारण स्वयं ही 'असत्य' की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तर्क, प्रयोग और अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि दो अतिवादी स्थितियों के मध्यमान पर ही 'सत्य' स्थित होता है, क्योंकि वही पर संतुलन और स्थायित्व उपलब्ध होते हैं। यह तथ्य स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि यह स्थायित्व जड़ता का सूचक नहीं है, वरन् । गतिशील संतुलन का, मध्यमान का गुण है।''
इस संतुलित मध्य स्थिति को प्राप्त करने में, जिसमें धार्मिक और वैज्ञानिक विचारधाराओं का आनुपातिक समन्वय हो जाता है, दर्शन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्रसन्नता की बात है कि सर्वोच्चकोटि के वैज्ञानिकों ने भी दर्शन की इस उपयोगिता को अब स्वीकार कर लिया है। परिणामस्वरूप मानवीय इतिहास का नया और कल्याणकारी युग प्रारंभ करने की सामर्थ्य से युक्त वैज्ञानिक और धार्मिक विज्ञान की प्रतिष्ठा स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
अंधश्रद्धा उपार्जित, कल्पना प्रभूत-अवास्तविकता पर आधारित धर्म स्वतंत्र इकाई के रूप में कितना हानिप्रद है-इसका अनुमान व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभावों को देखकर लगाया जा सकता है। गैलीलियो और आर्कमिडीज के प्राणहरण से लेकर धर्मोन्माद और धर्मयुद्ध तक, तथा परदा प्रथा से लेकर गलत कार्य (पाप) की अनिवार्य हानिकारक प्रतिक्रिया (दंड) तक मात्र स्नान द्वारा मक्ति तक सैकडों, सहस्त्रों धार्मिक अंधविश्वास और मूढ़मान्यताएँ धर्म के नाम पर मानव मस्तिष्क पर हावी हो गई हैं। गुरुडम नामक तानाशाही बैकुंठ निर्वाण दिलाने की दलाली आनुवंशिक उच्चता तथा प्रजातीय उच्चता का अहंकार जैसी अनेक अवैज्ञानिक मान्यताएँ व परंपराएँ धर्म की दुहाई देकर फल-फूल रही हैं। 'कारण-कार्य' का नियम एवं धार्मिक सिद्धांतों व नियमों का पुनः परीक्षण करने का प्रत्येक जिज्ञासु को अधिकार है। उनकी सुस्पष्ट एवं सर्वज्ञात विधि-व्यवस्था, प्रमाणित तथ्यों की मान्यता-जैसे वैज्ञानिक आधार धर्म व्यवस्था में ढूँढे नहीं मिलते, किंतु आशा की जानी चाहिए कि वैज्ञानिक धर्म जब कभी मानव समाज में प्रचलित होगा, तब क्यों-कैसे की कसौटियाँ ही धार्मिक सिद्धांतों व क्रियाकलापों की मान्यता और समाज में उनके प्रसारण की स्वीकृति का प्रमाण पत्र प्रदान किया करेंगी।
विज्ञान भी स्वतंत्र इकाई के रूप में कितना अपूर्ण है, इसकी झलक जेम्स जीन्स के इस वक्तव्य से मिलती है विज्ञान पूँगा और बहरा है। वह एक हथेली पर पैनिसिलीन और दूसरी पर परमाणु बम रखकर तुम्हारे पास आता है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम किसे पसंद करते और उठाते हो।' तात्पर्य यह हुआ कि विज्ञान चुनाव संबंधी कोई सलाह नहीं देता, न ही गलत चुनाव के दुष्परिणामों की शिकायत सुनना चाहता है।
तब सही मार्गदर्शन कहाँ प्राप्त हो? असमंजस की इस स्थिति में धर्म-वास्तविक धर्म-सहायता का हाथ बढ़ाता है। वह सत्य, न्याय और लोक-मंगल की कसौटियाँ प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक विज्ञानों की जो भी देन कसौटियों पर खरी उतरें, वे ही ग्रहणीय हैं, शेष नष्ट करने योग्य। जब कभी भी धार्मिक विज्ञान विश्व में प्रचलित होगा, उपर्युक्त कसौटियाँ ही अनुसंधान की दिशाओं को निश्चित किया करेंगी।
पदार्थ कितना ही मूल्यवान एवं उपयोगी क्यों न हो। उसकी कोई कीमत तभी है, जब चेतन प्राणी उसे उस प्रकार की मान्यता दे। अन्यथा वस्तु की दृष्टि से हीरा और कोयला लगभग एक ही स्तर के होते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से लोहा सोने की अपेक्षा अधिक कारगर है, पर मनुष्य ने जितनी मान्यता जिसको दी उसी अनुपात से उसका मूल्य बढ़ा है। पदार्थ अपनी उपयोगिता स्वयं सिद्ध नहीं कर सकते। मनुष्य की बुद्धि ही उन्हें खोजती है। और काम में लाने योग्य बनाती है। अस्तु, पदार्थ की तुलना में चेतना का महत्त्व अधिक हुआ, स्वयं विज्ञान का विकास भी बुद्धिकौशल की ही प्रतिक्रिया है। ऐसी दशा में चेतना के मूल अस्तित्व को स्वीकार न करना, उसे जड़-शरीर के सम्मिलन से उत्पन्न हलचल भर मानना, यही सिद्ध करता है कि वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र को आधा-अधूरा ही समझा है, जिसमें वे अपनी सारी अन्वेषण प्रक्रिया सँजोए हुए है।
पदार्थ विज्ञान की ही बात लें तो प्रतीत होगा कि उसकी खोज के साधन रूप में जड़ पदार्थों का ही उपयोग होता है। जिन यन्त्र उपकरणों के माध्यम से प्रकृतिगत हलचलों का पता लगाया जाता।
और उपलब्ध ज्ञान का उपयोग किया जाता है, वे स्वयं जड़ पदार्थों के बने हुए होते हैं। उसकी पकड़ और पहुँच अपनी सीमा तक ही काम कर सकती है। मस्तिष्क का सचेतन इंद्रियगम्य ज्ञान विशुद्ध भौतिकी है। इसे मन कहते हैं। जानकारियाँ प्राप्त करना और खोज कुरेद करना इसी का काम है। बुद्धि और अन्वेषण उपकरणों की सहायता से ही वैज्ञानिक खोजबीन का ढाँचा खड़ा किया जाता है। ऐसी दशा में चेतनसत्ता का वास्तविक स्वरूप और बल प्रकट नहीं हो सकता। उसके प्रकटीकरण में चेतना का वह भाग प्रयुक्त करना होता है, जिसे अंतर्मन, उच्च मन, अंतरात्मा, अतींद्रिय तत्त्व कहते हैं। ब्रह्मविद्या उसी की विवेचना करती है। तत्त्वदर्शन का आविष्कार इसी निमित्त हुआ है। ऋतंभरा प्रज्ञा, भूमा, धी इसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है। अतींद्रिय ज्ञान के सहारे ही चेतन तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर सकना संभव है। इसकी उपेक्षा करके जो विज्ञान काम में लाया जा रहा है, उसे अपर्ण ही कहना चाहिए।
वैज्ञानिक विचारक एडिंगटन ने इधर विज्ञान की इस मान्यता पर, कि वही वस्तुओं का सही-सही वर्णन कर सकता है, अनेक प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। अपनी पुस्तक'दि फिलासफी ऑफ फिजीकल साइंस' में उन्होंने कहा है कि जब हम अणुओं अथवा किसी तत्त्व के गुणों की चर्चा करते हैं तो ये गुण उन अणुओं या पुद्गल तत्त्वों के एकमात्र वास्तविक गुण कदापि नहीं माने जा सकते। अपितु ये तो वे गुण हैं, जिन्हें हमने अपनी प्रेक्षण-विधि द्वारा उन अणुओं या पुद्गल तत्त्वों पर आरोपित कर दिया है। इस प्रकार एडिंगटन ने निष्कर्ष निकाला है कि विज्ञान जिस जगत का वर्णन करता है, वह और भी अधिक आत्मपरक होता है, जबकि अभी तक कथित पदार्थवादी या वैज्ञानिक भौतिकतावादी इसी बात पर जोर देते थे कि अध्यात्मवादियों का संपूर्ण चिंतन आत्मनिष्ठ होता है, वस्तुपरक नहीं और वस्तुपरक चिंतन तो मात्र विज्ञान द्वारा ही संभव है।
एडिंगटन ने अपनी बात एक उदाहरण द्वारा समझाई है। उनका कहना है कि जिस प्रकार एक मछुआ कुछ मछलियों को पकड़ता है, फिर वह वर्णन करता है कि मछलियाँ इस-इस तरह की होती हैं तो मछुए का यह वर्णन सिर्फ उन्ही मछलियों पर लागू होता है, जिन्हें उसने पकड़ा है। उसी प्रकार भौतिकशास्त्र का विश्व संबंधी ज्ञान केवल उन्हीं वस्तुओं पर लागू हो सकता है, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों, उपकरणों तथा बुद्धि की पकड़ में ला सकते हैं। इस प्रकार भौतिकशास्त्र में जिसे हम सामान्य कथन या प्रकृति के नियम कहते हैं, वे एक ऐसे सार का वर्णन हैं, जो हमारे अपने बोध पर निर्भर है। इसे ही एडिंगटन 'चयनात्मक आत्मनिष्ठतावाद' (सलेक्टिव सब्जेक्टिविज्म) कहते हैं।
इसलिए जानसन ने 'फ्राम दि फिजीकल टू दि सोशल साइंसेज' में लिखा है-'हमारे पास यह कहने का कोई आधार नहीं है कि भौतिकशास्त्र के सिद्धांत जिन कारणों का उद्घाटन करते हैं वे वस्तुओं की असली प्रकृति हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को लें, इनकी असली प्रकृति क्या है? यह पूरी तरह कोई वैज्ञानिक नहीं कह सकता। जिस रूप में इनका वर्णन किया जाता हैं, वह वैज्ञानिकों के विभिन्न प्रेक्षणों (आब्जर्वेसंस) को संबद्ध करने के लिए आवश्यक गुण मात्र हैं। इनकी वास्तविक सत्ता का पूर्ण विवरण ज्ञात नहीं है।
विज्ञान के द्वारा आविष्कृत इस 'अनिश्चयात्मकता' ने आज जहाँ एक ओर ऐसे 'दर्शन' को जन्म दिया है, जो दर्शनशास्त्र' मात्र के विरोधी हैं तथा जिनका कहना है कि सृष्टि संबंधी कोई भी दार्शनिक-समीक्षा मात्र परिकल्पनात्मक होती है, उसकी वास्तविकता की जाँच संभव नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों के पैर उखाड़ दिए हैं।
विटगेन्स्टाइन तथा अन्य तर्कमूलक भाववादियों (लाजिकल पाजिटिह्विस्ट्स) की मान्यता है कि प्रकृति के नियम सामान्य कथन नहीं हो सकते, बल्कि वे ‘प्रोपोजीशनल फंक्शन' मात्र होते हैं।
उनके द्वारा वर्तमान मूल्यों के विभिन्न मान रखकर परीक्षण के लिए विशेष कथन तो प्राप्त किए जा सकते हैं, पर कोई सामान्य कथन नहीं निकाले जा सकते, जबकि वैज्ञानिक प्रवर आइन्स्टाइन मानते थे कि प्रत्येक वैज्ञानिक इसे निश्चित धारणा के साथ ही अनुसंधान करता है कि यह विश्व एक सुसंगत तथा कारण-कार्यमूलक इकाई है। देखने में ये दोनों निष्कर्ष परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, पर ये वैसे हैं नहीं। ये वस्तुतः यथार्थ के दो भिन्न-भिन्न स्तरों के भिन्न-भिन्न विश्लेषण हैं।
आज विज्ञान भी यथार्थ एवं आभास का अंतर कहाँ मान रहा है। वेदांत-मत में इसे ही पारमार्थिक सत्य तथा व्यावहारिक सत्य के रूप में विश्लेषित किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा यथार्थ का यह परीक्षण कि सृष्टि की मूलसत्ता उस रूप में नहीं है, जैसे कि व्यवहारतः हम जानते-मानते हैं, वेदांत के सर्वदा अनुरूप है। यह ध्यान रहे कि वैज्ञानिक यह कतई नहीं मानते कि विश्व कुछ है ही नहीं और सब 'शून्य' है।
एडिंगटन ने ‘न्यू पाथवेज इन साइंस' नामक ग्रंथ में स्पष्ट कहा है-''मेरा तात्पर्य यह कदापि नहीं कि भौतिक विश्व का अस्तित्व ही नहीं है।'' वस्तुतः भौतिक विश्व व्यवहारतः पूर्ण सत्य है, उसमें एक निश्चित विधि-व्यवस्था है, क्रमबद्धता है। अनिश्चित सिद्धांत का भी यह अर्थ नहीं कि इस दुनिया में सभी कुछ अनिश्चित है। इससे सर्वथा विपरीत वैज्ञानिकों और वेदांतियों का यह मत है कि सृष्टि में सर्वत्र कारण-कार्य भाव विद्यमान है। प्रत्येक कार्य का एक निश्चित कारण है। अनिश्चित के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा हम सृष्टि की मूलसत्ता को पूरी तरह कभी नहीं जान सकते, क्योंकि प्रयोग के उपकरण और माध्यम भी उसी सृष्टि के अंश है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।
वैज्ञानिक विश्लेषणों के तीन मुख्य दार्शनिक निष्कर्ष हैं
(१) ब्रह्मांड का आदि कारण कोई अतिसूक्ष्म एकमेव सत्ता है, जो चेतन है, किंतु पूरी तरह पदार्थविहीन नहीं। तरंगों का जो रूप ज्ञात हुआ है, वह प्रकृति की मूल शक्ति के सापेक्ष स्वरूप को स्पष्ट करता है। प्रकृति की यह मूलशक्ति वेदांत-विचार की माया की तरह अवरार्ध, अव्याख्येय है। शुद्ध माया या मूलशक्ति तो चेतन से घनिष्ठता से संबद्ध है, पर स्वयं चैतन्यमात्र नहीं। वह पूरी तरह द्रव्यातीत नहीं।
(२) सृष्टि का ठीक-ठीक स्वरूप जाना नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे ज्ञान की सीमाएँ है। उसके द्वारा हम उससे परे का यथार्थ नहीं जान सकते।
(३) वैज्ञानिकों का तीसरा निष्कर्ष यह है कि भौतिक विश्व आभास का (एपियरेन्स का) क्षेत्र है, यथार्थ का नहीं। यथार्थ उसकी पृष्ठभूमि में है। अर्थात विश्व की व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक या परम यथार्थ सत्ता नहीं है। स्पष्टतः यह वेदांत मत के अनुसार है।
अपनी पुस्तक "दि न्यू बैकग्राउंड ऑफ साइंस'' में सर जेम्स जीन्स ने भी कहा है, सृष्टि में हम जो विधि-व्यवस्था पाते हैं, वे अत्यंत स्पष्टता तथा सरलता से आइडियलिज्म की भाषा में वर्णितव्याख्यायित हैं।
यथार्थ और आभास (रियलिटी एण्ड अपियरेन्स) की विवेचना करते हुए वैज्ञानिक अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रकृति को हम पूरी तरह कभी भी जान नहीं सकेंगे। उसका मूलस्वरूप सदा ही अज्ञात रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम जानने की चेष्टा करते हैं, हम उसमें 'व्यवधान' उपस्थित करने लगते हैं। इसलिए महान वैज्ञानिक हाइजन बर्ग ने 'अनिश्चय का सिद्धांत' प्रतिपादित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी माध्यम के द्वारा फिर वह प्रकाश हो, ऊर्जा हो या कुछ और जैसे ही हम ‘मैटर' के किसी अंश से संपर्क करते हैं, हम उसके प्राकृतिक स्वरूप में व्यवधान उपस्थित कर देते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का असली स्वरूप क्या है, यह कभी भी नहीं जाना जा सकता, हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति एव वेग का प्रकाश की सहायता से सूक्ष्म उपकरणों द्वारा परीक्षण करते हैं तो प्रकाश का यह सहयोग कथित इलेक्ट्रॉन की स्वाभाविक दशा को निश्चित ही प्रभावित कर देता होगा। फिर परीक्षण के लिए प्रयुक्त उपकरण भी उसी सृष्टि के एक अंश हैं, जिनके द्वारा कि उस सृष्टि का रहस्य जानने का प्रयास किया जा रहा होता है। इन उपकरणों का संपर्क परीक्षित किए जा रहे अंश को स्वाभाविक नहीं रहने दे सकता। इस प्रकार प्रयोगों द्वारा यथार्थसत्ता का ज्ञान असंभव है।
जगत का स्वरूप समझने की वैज्ञानिक विधि इंद्रिय ज्ञान तक सीमित है। सूक्ष्मदर्शी यन्त्रों द्वारा एकत्र जानकारी मस्तिष्क को इंद्रियों द्वारा ही मिलती है। स्थूल दृश्य जगत की यथार्थता जानने-समझने में ही हमारी ज्ञानेंद्रियाँ बराबर धोखा खाती रहती हैं, मस्तिष्क भी पगपग पर भ्रम में पड़ता रहता है। स्पष्ट है कि इन आधारों पर जब प्रत्यक्ष-जगत के बारे में ही सही निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं, तो अदृश्य सूक्ष्म जगत में तो हमारी सीमाएँ स्पष्ट हैं। अणुसंरचना के स्पष्टीकरणों द्वारा जो जानकारी और सहायता एकत्र की गई है, उससे अधिक आश्रय अनुमान पर आधारित गणितपरक आधारों का लिया गया है, तभी कुछ निष्कर्ष निकाले जा सके हैं।
यथार्थ की तह तक पहुँचने के लिए, सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए परख के आधार को अधिक विस्तृत करना होगा। इस दिशा में विज्ञान के प्रयास चल पड़े हैं।
इस तरह से अच्छा हो, यदि हम धर्म को 'अपूर्ण विज्ञान' कहें और विज्ञान को 'अपूर्ण धर्म'। यह पर्यायवाची शब्द जहाँ उनकी निजी विशेषताओं पर जरा भी आँच नहीं लाते। वहीं उनकी अपूर्णता और अन्योन्याश्रितता को भी उभारकर हमारे सामने लाते हैं और हमारी भ्रांति को दूर करते हैं कि उनमें कोई एक प्रमुख और प्रभावशाली है तथा दूसरा गौण और मुखापेक्षी।
वास्तविकता यह है कि मानव रचना में आत्मतत्त्व और अनात्मतत्त्व दोनों लगे हैं। दोनों के तालमेल से ही जीवन सुसंगठित, संतुलित और उन्नत हो सकता है। आत्म विज्ञान और पदार्थ विज्ञान दोनों का समानुपातिक समन्वय ही इहलोक और परलोक को उत्साह व समृद्धि से तथा संतोष व आनंद से भर सकता है। धर्म और विज्ञान का–अर्थात आत्मा और अनात्म पक्षों का, परमात्मा और माया का, आत्मकल्याण और विश्वकल्याण का, परलोक और इहलोक का ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण योग ही व्यावहारिक और उचित है।
पिछले कुछ समय की तथा वर्तमान समय की धर्म और विज्ञान के क्षेत्रों की गतिविधियाँ इस बात का संकेत दे रही हैं कि उनके बीच की कृत्रिम दीवारों के ढहने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पूर्वकाल में धर्म द्वारा निंदित और दंडित विज्ञान आज धर्म से हाथ मिलाकर उसे अपनी वैज्ञानिकता प्रदान कर रहा है, दूसरी ओर धर्म के शाश्वत सिद्धांत ने सर्वोच्च कोटि के वैज्ञानिकों के चिंतन को परम सत्य की शोध तथा मानव कल्याण के प्रयास की दिशा में बढ़ने की सफल प्रेरणा दी है। प्रकृति के मूलभूत नियमों की खोज, परामनोविज्ञान आदि धर्म और विज्ञान के मध्य सेतु बनने जा रहे हैं। इस बात के लक्षण दिखाई देने लगे है कि संपूर्ण मानवता की एक आत्मा की घोषणा करने वाला वैज्ञानिक धर्म भविष्य के गर्भ में विकसित हो रहा है। विभिन्न विशिष्ट विज्ञान भी परस्पर समन्वित होकर एक विज्ञान का रूप धारण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आशा की जानी चाहिए कि ऐसा समन्वित विज्ञान स्वयं को तथा धर्म को एक ही वृहद् सत्य के दो परस्पर संबंधित पक्ष सिद्ध कर सकेगा। अविच्छिन्न रूप से जुड़े तथा एकदूसरे को पोषित करने वाले धर्म और विज्ञान की, अर्थात वैज्ञानिक धर्म और धार्मिक विज्ञान की आज के विश्व में महती आवश्यकता है। इनके प्रादुर्भाव और क्रियाशील होने के पश्चात् ही विश्वशांति और विश्वबंधुत्व की कल्पनाएँ सार्थक हो सकेंगी।
|
|||||


 i
i