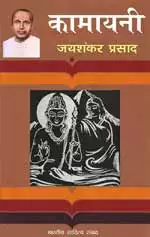|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
नहीं पा सका हूं मैं जैसे
जो तुम देना चाह रही,
क्षुद्र पात्र! तुम उसमें
कितनी मधु-धारा हो ढाल रही।
सब बाहर होता जाता है
स्वगत उसे मैं कर न सका,
बुद्धि-तर्क के छिद्र हुए
थे हृदय हमारा भर न सका।
यह कुमार-मेरे जीवन का
उच्च-अंश, कल्याण-कला।
कितना बड़ा प्रलोभन मेरा
हृदय स्नेह बन जहां ढला।
सुखी रहें, सब सुखी रहें
बस छोड़ो मुझ अपराधी को,
श्रद्धा देख रही चुप मनु
के भीतर उठती आंधी को।
दिन बीता रजनी भी तंद्रा
निद्रा संग लिये।
इड़ा कुमार समीप पड़ी थी मन
की दबी उमंग लिये।
श्रद्धा भी कुछ खिन्न
थकी-सी हाथों का उपधान किये,
पड़ी सोचती मन ही मन कुछ,
मनु चुप सब अभिशाप पिये-
सोच रहे थे, ''जीवन सुख
है? ना, यह विकट पहेली है,
भाग अरे मनु! इंद्रजाल से
कितनी व्यथा न झेली है?
यह प्रभात को स्वर्ण
किरण-सी झिलमिल चंचल सी छाया,
श्रद्धा को दिखलाऊं कैसे
यह मुख या कलुषित काया।
और शत्रु सब, ये कृतघ्न
फिर इनका क्या विश्वास करूं,
प्रतिहिंसा प्रतिशोध दबा
कर मन ही मन चुपचाप मरूं।
श्रद्धा के रहते यह संभव
नहीं कि कुछ कर पाऊंगा,
तो फिर शांति मिलेगी
मुझको जहां, खोजता जाऊंगा।''
जगे सभी जब नव प्रभात में
देखें तो मनु वहां नहीं,
'पिता कहां' कह खोज रहा
सा यह कुमार अब शांत नहीं।
इड़ा आज अपने को सबसे
अपराधी है समझ रही,
कामायनी मौन बैठी-सी अपने
में ही उलझ रही।
0 0 0
|
|||||


 i
i