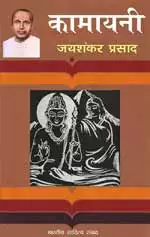|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
तारा बनकर यह बिखर रहा
क्यों स्वप्नों का उन्माद अरे!
मादकता-माती नींद लिए
सोऊं मन में अवसाद भरे।
चेतना शिथिल-सी होती है
उन अंधकार की लहरों में-''
मनु डूब चले धीरे-धीरे
रजनी के पिछले पहरों में।
उस दूर क्षितिज में
सृष्टि बनी स्मृतियों की संचित छाया से,
इस मन को है विश्राम
कहां! चंचल यह अपनी माया से।
जागरण-लोक था भूल चला
स्वर्णों का सुख-संचार हुआ,
कौतुक-सा बन मनु के मन का
वह सुंदर क्रीड़ागार हुआ।
था व्यक्ति सोचता आलस में
चेतना सजग रहती दुहरी,
कानों के कान खोल करके
सुनती थी कोई ध्वनि गहरी :-
''प्यासा हूं, मैं अब भी
प्यासा संतुष्ट ओथ से मैं न हुआ,
आया फिर भी वह चला गया
तृष्णा को तनिक न चैन हुआ।
देवों की सृष्टि विलीन
हुई अनुशीलन में अनुदिन मेरे,
मेरा अतिचार न बंद हुआ
उन्मत्त रहा सबको घेरे।
मेरी उपासना करते वे मेरा
संकेत विधान बना,
विस्मृत जो मोह रहा मेरा
वह देव-विलास-वितान तना।
मैं काम, रहा सहचर उनका
उनके विनोद का साधन था,
हंसता था और हंसाता था
उनका मैं कृतिमय जीवन था।
जो आकर्षण बन हंसती थी
रति थी अनादि-वासना वही,
अव्यक्त-प्रकृति-उन्मीलन
के अंतर में उसकी चाह रही।
|
|||||


 i
i