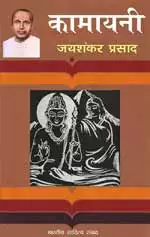|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
श्रद्धा अपनी शयन-गुहा
में दुखी लौट कर आयी,
एक विरक्ति-बोझ सी ढोती
मन ही मन बिलखायी।
सुखी काष्ठ सीध में पतली
अनल शिखा जलती थी,
उस धुंधले गृह में आभा
से, तामस को छलती थी।
किंतु कभी बुझ जाती पाकर
शीत पवन के झोंके,
कभी उसी से जल उठती तब
कौन उसे फिर रोके?
कामायनी पड़ी थी अपना कोमल
चर्म बिछा के,
श्रम मानो विश्राम कर रहा
मृदु आलस को पाके।
धीरे-धीरे जगत चल रहा
अपने इस उस ऋजुपथ में,
धीरे-धीरे खिलते तारे मृग
जुतते विधुरथ में!
अंचल लटकाती निशीथिनी
अपना ज्योत्सना-शाली,
जिसकी छाया में सुख पावे
सृष्टि वेदना वाली,
उच्च शैल-शिखरों पर हंसती
प्रक्रति चंचला बाला,
धवल हंसी बिखराती अपना
फैला मधुर उजाला।
जीवन की उद्दाम लालसा
उलझी जिसमें व्रीड़ा,
एक तीव्र उन्माद और मन
मथने वाली पीड़ा।
मधुर विरक्ति-भरी आकुलता,
घिरती हृदय-गगन में,
अंतदहि स्नेह का तब भी
होता था उस मन में।
वे असहाय नयन थे
खुलते-मुंदते भीषणता में।
आज स्नेह का पात्र खड़ा था
स्पष्ट कुटिल कटुता में।
''कितना दु:ख जिसे मैं
चाहूं वह कुछ और ही बना हो,
मेरा मानस-चित्र खींचना
सुंदर-सा सपना हो।
|
|||||


 i
i