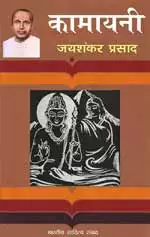|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
मनु ने देखा जब श्रद्धा
का वह सहज-खेद से भरा रूप,
अपनी इच्छा का दृढ़
विरोध-जिसमें वे भाव नहीं अनूप।
वे कुछ भी बोले नहीं, रहे
चुपचाप देखते साधिकार,
श्रद्धा कुछ-कुछ मुस्कुरा
उठी ज्यों जान गई उनका विचार।
'दिन भर थे कहां भटकते
तुम' बोली श्रद्धा भर मधुर स्नेह-
''यह हिंसा इतनी है
प्यारी जो भुलवाती है देह-गेह।
मैं यहां अकेली देख रही
पथ, सुनती-सी पद-ध्वनि नितांत,
कानन में जब तुम दौड़ रहे
मृग के पीछे बन कर अशांत!
ढल गया दिवस पीला-पीला
तुम रक्तारुण बन रहे धूम,
देखो नीड़ों में विहग-युगल
अपने शिशुओं को रहे चूम!
उनके घर में कोलाहल है
मेरा सूना है गुफा-द्वार!
तुमको क्या ऐसी कमी रही
जिसके हित जाते अन्य-द्वार?''
''श्रद्धे तुमको कुछ कमी
नहीं पर मैं तो देख रहा अभाव,
भूली-सी कोई मधुर वस्तु
जैसे कर देती विकल घाव।
चिर-मुक्त-पुरुष वह कब
इतने अबरुद्ध श्वास लेगा निरीह!
गतिहीन पंगु-सा पड़ा-पड़ा
ढह कर जैसे बन रहा डीह।
जब जड़-बंधन-सा एक मोह
कसता प्राणों का मृदु शरीर,
आकुलता और जकड़ने की तब
ग्रंथि तोड़ती हो अधीर।
हंस कर बोले, बोलते हुए
निकले मधु-निर्झर-ललित-गान,
गानों में हो उल्लास भरा
झूमे जिसमें बन मधुर प्रान।
|
|||||


 i
i