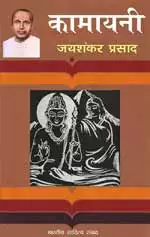|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
स्वयं देव थे हम सब, तो
फिर क्यों न विश्रृंखल होती सृष्टि?
अरे अचानक हुई इसी से कड़ी
आपदाओं की वृष्टि।
गया, सभी कुछ गया, मधुर
तम सुर-बालाओं का श्रृंगार,
उषा ज्योत्स्ना-सा
यौवन-स्मित मधुप-सदृश निश्चित विहार।
भरी वासना-सरिता का वह
कैसा था मदमत्त प्रवाह,
प्रलय-जलधि में संगम
जिसका देख हृदय था उठा कराह।''
''चिर-किशोर-वय,
नित्यविलासी-सुरभित जिससे रहा दिगंत,
आज तिरोहित हुआ कहां वह
मधु से पूर्ण अनंत वसंत?
कुसुमित कुंजों में वे
पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन,
मौन हुई है मूर्च्छित
तानें और न सुन पड़ती अब बीन।
अब न कपोलों पर छाया-सी
पड़ती मुख की सुरभित भाप,
भुज-भूलों में शिथिल वसन
की व्यस्त न होती है अब माप।
कंकण क्वणित, रणित नृपुर
थे, हिलते थे छाती पर हार,
मुखरित था कलरव, गीतों
में स्वर लय को होता अभिसार।
सौरभ से दिगंत पूरित था,
अंतरिक्ष आलोक-अधीर,
सब में एक अचेतन गति थी,
जिससे पिछड़ा रहे समीर।
वह अनंग-पीड़ा-अनुभव-सा
अंग-भगियों का नर्तन,
मधुकर के मरंद-उत्सव-सा
मदिर भाव से आवर्तन।
सुरा सुरभिमय बदन अरुण से
नयन भरे आलस अनुराग,
कल कपोल था जहाँ बिछलता
कल्पवृक्ष का पीत पराग।
|
|||||


 i
i