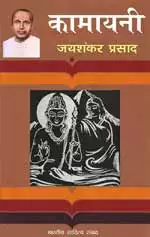|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
स्वप्न
संध्या अरुण जलज केसर ले अब तक मन थी बहलाती,मुरझा कर कब गिरा तामरस उसको खोज कहां पाती!
क्षितिज भाल का कुंकुम मिटता मलिन कालिमा के कर से,
कोकिल की काकली वृथा ही अब कलियों पर मंडराती।
कामायनी-कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरंद रहा,
एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहां!
वह प्रभात का हीनकला शशि-किरन कहां चांदनी रही,
वह संध्या थी - रवि, शशि, तारा ये सब कोई नहीं जहां।
जहां तामरस इंदीवर या सित शतदल हैं मुरझाये –
अपने नालों पर, वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुप आये।
वह जलधर जिसमें चपला या श्यामलता का नाम नहीं,
शिशिर-कला की क्षीण-स्रोत वह जो हिमतल में जम जाये।
एक मौन वेदना विजन की, झिल्ली की झनकार नहीं
जगती की अस्पष्ट - उपेक्षा, एक कसक साकार रही।
हरित-कुंज की छाया भर-थी वसुधा-आलिंगन करती,
वह छोटी सी विरह-नदी थी जिसका है अब पार नहीं।
नील गगन में उड़ती-उड़ती विहग-बालिका सी किरणें,
स्वप्न-लोक को चलीं थकी सी नींद-सेज पर जा गिरने।
किंतु, विरहिणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं –
बिजली-सी स्मृति चमक उठी तब, लगे अभी तम-घन घिरने।
संध्या नील सरोरुह से जो श्याम पराग बिखरते थे,
शैल-घाटियों के अंचल को वे धीरे से भरते थे।
तृण-गुल्मों से रोमांचित नग सुनते उस दुख की गाथा
श्रद्धा की सूनी सांसों से मिलकर जो स्वर भरते थे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i