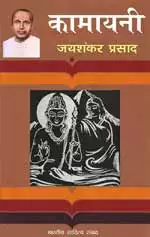|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
किंतु स्वयं भी क्या वह
साथ कुछ मान चलूं मैं,
तनिक न मैं स्वच्छंद,
स्वर्ण सा सदा गलूं मैं!
जो मेरी है सृष्टि उसी से
भीत रहूं मैं,
क्या अधिकार नहीं कि कभी
अविनीत रहूं मैं?
श्रद्धा का अधिकार समर्पण
दे न सका मैं
प्रतिफल बढता हुआ कब वहां
रुका मैं।
इड़ा नियम-परितंत्र चाहती
मुझे बनाना
निर्वाधित अधिकार उसी एक
न माना।
विश्व के बंधन विहीन
परिर्वतन तो है,
इसकी गति में
रवि-शशि-तारे ये सब जो हैं।
रूप बदलते रहते वसुधा
जलनिधि बनती,
उदधि बना मरुभूमि जलधि
में ज्वाला जलती!
तरल अग्नि की दौड़ लगी है
सब के भीतर,
गल कर बहते हिम-नग
सरिता-लीला रच कर।
यह स्फुलिंग का नृत्य एक
पल आया बीता!
टिकने को कब मिला किसी को
यहां सुभीता?
कोटि-कोटि नक्षत्र शून्य
के महा-विवर में,
लास रास कर रहे लटकते हुए
अधर में।
उठती है पवनों के स्तर
में लहरें कितनी,
यह असंख्य चीत्कार और
परवशता इतनी।
|
|||||


 i
i