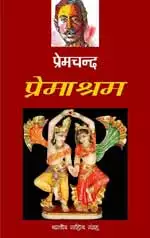|
सदाबहार >> प्रेमाश्रम (उपन्यास) प्रेमाश्रम (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
370 पाठक हैं |
||||||||
‘प्रेमाश्रम’ भारत के तेज और गहरे होते हुए राष्ट्रीय संघर्षों की पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है
मनोहर– फिर बीच में बोला?
बलराज– क्यों न बोलूँ, तुम तो दो-चार दिन के मेहमान हो, जो कुछ पड़ेगी। वह तो हमारे ही सिर पड़ेगी। ज़मींदार कोई बादशाह नहीं है कि चाहे जितनी जबरदस्ती करे और वह मुँह न खोलें। इस जमाने में तो बादशाहों का भी इतना अख्तियार नहीं, ज़मींदार किस गिनती में हैं! कचहरी दरबार में कहीं सुनायी नहीं है तो (लाठी दिखलाकर) यह तो कहीं नहीं गयी है।
डपट– कहीं खाँ साहब यह बातें सुन लें तो गजब हो जाय।
बलराज– तुम खाँ साहब से डरो, यहाँ उनके दबैल नहीं हैं। खेत में चाहे कुछ उपज हो या न हो, बेसी होती चली जाय, ऐसा क्या अन्धेर है? ‘सरकार के घर कुछ तो न्याय होगा, किस बात पर बेसी मंजूर करेगी।
डपट– अनाज का भाव नहीं चढ़ गया है?
बलराज– भाव चढ़ गया है तो मजदूरों की मजदूरी भी चढ़ गयी है, बैलों का दाम भी तो चढ़ गया है, लोहे-लक्कड़ का दाम भी तो चढ़ गया है, यह किसके घर से आयेगा?
इतने में तो कादिर मियाँ घास का गट्ठर सिर पर रखे हुए आकर खड़े हो गये। बलराज की बातें सुनीं तो मुस्कुराकर बोले– भाँग का दाम भी तो चढ़ गया है। चरस भी महँगी हो गई है, कत्था-सुपारी भी तो दूने दामों बिकती है, इसे क्यों छोड़ जाते हो?
मनोहर– हाँ, कदारि दादा, तुमने हमारे मन की कही।
बलराज– तो क्या अपनी जवानी में तुम लोगों ने बूटी-भाँग न पी होगी? या सदा इसी तरह एक जून चबेना और दूसरी जून रोटी-साग खाकर दिन काटे हैं? और फिर तुम ज़मींदार के गुलाम बने रहो तो उस जमाने में और कर ही क्या सकते थे? न अपने खेत में काम करते, किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करते। अब तो शहरों में मजूरों की माँग है, रुपया रोज खाने को मिलता है, रहने को पक्का घर अलग। अब हम जमींदारों की धौंस क्यों सहें, क्या भर पेट खाने को तरसें?
कादिर– क्यों मनोहर, क्या खाने को नहीं देते?
बलराज– यह भी कोई खाना है कि एक आदमी खाय और घर के सब आदमी उपास करें? गाँव में सुक्खू चौधरी को छोड़कर और किसी के घर दोनों बेला चूल्हा जलता है? किसी को एक जून चबेना मिलता है, कोई चुटकी भर सत्तू फाँककर रह जाता है। दूसरी बेला भी पेट भर रोटी नहीं मिलती।
|
|||||


 i
i