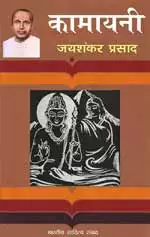|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
''श्रद्धा! तू आ गयी भला
तो-पर क्या मैं था यहीं पड़ा!''
वही भवन, ये स्तंभ,
वेदिका! बिखरी चारों ओर बुणा।
आंख बंद कर लिया क्षोभ से
''दूर-दूर से चल मुझको,
इस भयावने अंधकार में खो
दूं कहीं न फिर तुझको।
हाथ पकड़ ले, चल सकता
हूं-हां कि यही अवलंब मिले,
वह तू कौन? परे हट,
श्रद्धे! आ कि हृदय का कुसुम खिले।''
श्रद्धा नीरव सिर सहलाती
आंखों में विश्वास भरे,
मानो कहती ''तुम मेरे हो
अब क्यों कोई वृथा डरे?''
जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए
से लगे बहुत धीरे कहने,
''ले चल इस छाया के बाहर
मुझको दे न यहां रहने।
मुक्त नील नभ के नीचे या
कहीं गुहा में रह लेंगे,
अरे झेलता ही आया हूं -
जो आवेगा सह लेंगे।''
''ठहरो कुछ तो बल आने दो
लिवा चलूंगी तुरत तुम्हें,
इतने क्षण तक ''श्रद्धा
बोली-''रहने देंगी क्या न हमें?''
इड़ा संकुचित उधर खड़ी थी
यह अधिकार न छीन सकी,
श्रद्धा अविचल, मनु अब
बोले उनकी वाणी नहीं रुकी।
''जब जीवन में साध भरी थी
उच्छृंखल अनुरोध भरा,
अभिलाषायें भरी हृदय में
अपनेपन का बोध भरा।
मैं था, सुंदर कुसुमों की
वह सघन सुनहली छाया थी,
मलयानिल की लहर उठ रही
उल्लासों की माया थी!''
उषा अरुण प्याला भर लाती
सुरभित छाया के नीचे
मेरा यौवन पीता सुख से
अलसाई आंखें मींचे।
ले मकरंद नया चू पड़ती
शरद-प्रात की शेफाली,
बिखराती सुख ही, संध्या
की सुदर अलकें घुंघराली।
सहसा अंधकार की आंधी उठी
क्षितिज से वेग भरी,
हलचल से विक्षुब्ध विश्व
- थी उद्वेलित मानस लहरी।
व्यथित हृदय उस नीले नभ
में छायापथ-सा खुला तभी,
अपनी मंगलमयी मधुर-स्मिति
कर दी तुमने देवि! जभी।
|
|||||


 i
i