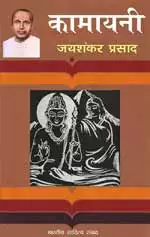|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
गिरि-निर्झर चले उछलते
छायी फिर से हरियाली,
सूखे तरु कुछ मुलक्याये
फूटी पल्लव में लाली।
वे युगल यहीं अब बैठे
संसृति की सेवा करते,
संतोष और सुख देकर सब की
दुख ज्वाला हरते।
है वहां महाहृद निर्मल मन
जो मन की प्यास बुझाता,
मानस उसको कहते हैं सुख
पाता जो है जाता।
''तो यह वृष क्यों तू यों
ही वैसे ही चला रही है,
क्यों न बैठ जाती इस पर
अपने को थका रही है?''
''सारस्वत-नगर-निवासी हम
आये यात्रा करने
यह व्यर्थ रिक्त-जीवन-घट
पीयूष-सलिल से झरने।
इस वृषभ धर्म-प्रतिनिधि
को उत्सर्ग करेंगे जाकर,
चिर-मुक्त रहे यह निर्भय
स्वच्छंद सदा-सुख पाकर।''
सब सम्हल गये थे आगे थी
कुछ नीची उतराई,
जिस समतल घाटी में, वह थी
हरियाली से छाई।
श्रम, ताप और पथ-पीड़ा
क्षण भर में थे अंतर्हित,
सामने विराट धवल-नग अपनी
महिमा से विलसित।
उसकी तलहटी मनोहर श्यामल
तृण-वीरुध वाली,
नव-कुंज, गुहा-गृह सुंदर
हद से भर रही निराली,
वह मंजरियों का कानन कुछ
अरुण पीत हरियाली,
प्रति-पर्व सुमन-संकुल थे
छिप गई उन्हीं में डाली।
|
|||||


 i
i