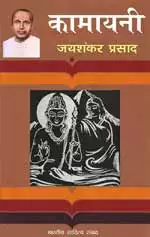|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
चन्द्र की विश्राम राका
बालिका-सी कांत,
विजयिनी सी दीखती तुम
माधुरी-सी शांत।
पददलित-सी थकी व्रज्या
ज्यों सदा आक्रांत,
शस्य-श्यामल भूमि में
होती समाप्त अशांत।
आह! वैसा ही हृदय का बन
रहा परिणाम,
पा रहा हूं आज देकर
तुम्हीं से निज काम।
आज ले लो चेतना का यह
समर्पण दान।
विश्व-रानी! सुन्दरी
नारी! जगत को मान!''
धूम-लतिका-सी गगन-तरु पर
न चढ़ती दीन,
दबी शिशिर-निशीथ में
ज्यों ओस-भार नवीन।
झुक चली सव्रीड़ वह
सुकुमारता के भार,
लद गई पाकर पुरुष का
नर्ममय उपचार।
और वह नारीत्व का जो मूल
मधु अनुभाव,
आज जैसे हंस रहा भीतर
बढ़ाता चाव।
मधुर व्रीड़ा-मिश्र चिंता
साथ ले उल्लास,
हृदय का आनन्द-कूजन लगा
करने रास।
गिर रहीं पलकें, झुकी थी
नासिका की नोक,
भ्रूलता थी कान तक चढ़ती
रही बेरोक।
स्पर्श करने लगी लज्जा
ललित कर्ण कपोल,
खिला पुलक कदंब सा था भरा
गद्गद् बोल।
किन्तु बोली ''क्या
समर्पण आज का हे देव!
बनेगा - चिर-बन्ध -
नारी-हृदय-हेतु - सदैव।
आह मैं दुर्बल, कहो क्या
ले सकूंगी दान!
वह, जिसे उपभोग करने में
विकल हों प्रान?''
0 0 0
|
|||||


 i
i