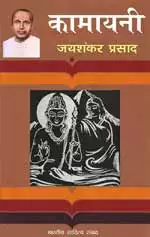|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
था एक पूजता देह दीन
दूसरा अपूर्ण अहंता में
अपने को समझ रहा प्रवीण,
दोनों हठ था दुर्निवार,
दोनों ही थे विश्वास-हीन।
फिर क्यों न तर्क को
शस्त्रों से वे सिद्ध करें-क्यों हो न युद्ध,
उनका संघर्ष चला अशांत वे
भाग रहे अब तक विरुद्ध,
मुझमें ममत्वमय आत्म-मोह
स्वातंत्र्यमयी उच्छृंखलता,
हो, प्रलय-भीत तन रक्षा
में पूजन करने की व्याकुलता।
वह पूर्व द्वंद्व
परिवर्तित हो मुझको बना रहा अधिक दीन,
सचमुच मैं हूं
श्रद्धा-विहीन।''
''मनु! तुम श्रद्धा को
गये भूल
उस पूर्ण आत्म-विश्वासमयी
को उड़ा दिया समझ तूल,
तुमने तो समझा असत् विश्व
जीवन धागे में रहा झूल।
जो क्षण बीतें सुख-साधन
में उनको ही वास्तव लिया मान,
वासना-तृप्ति ही स्वर्ग
बनी, यह उलटी मत्ति का व्यर्थ-ज्ञान।
तुम भूल गये पुरुषत्व-मोह
में कुछ सत्ता है नारी की,
समरसता है संबंध बनी
अधिकार और अधिकारी की।''
जब गूंजी यह वाणी तीखी
कंपित करती अंबर अकूल,
मनु को जैसे चुभ गया शूल।
''यह कौन? अरे फिर वही
काम!
जिसने इस भ्रम में है
डाला छीना जीवन का सुख-विराम?
प्रत्यक्ष लगा होने अतीत
जिन घड़ियों का अब शेष नाम।
वरदान आज उस गतयुग का
कंपित करता है अंतरंग,
अभिशाप ताप की ज्वाला से
जल रहा आज मन और अंग-
बोले मनु- ''क्या मैं
भ्रात साधना में ही अब तक लगा रहा,
क्या तुमने श्रद्धा की
पाने के लिए नहीं सस्नेह कहा?
पाया तो उसने भी मुझको दे
दिया हृदय निज अमृत-धाम,
फिर क्यों न हुआ मैं
पूर्ण-काम?''
|
|||||


 i
i