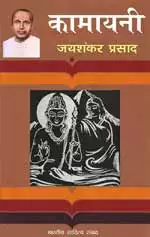|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
जीवन सारा बन जाय युद्ध
उस रक्त अग्नि की वर्षा
में बह जायं सभी जो भाव शुद्ध,
अपनी शंकाओं से व्याकुल
तुम अपने ही होकर विरुद्ध।
अपने को आवृत किये रहो
दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप,
वसुधा के समतल पर उन्नत
चलता फिरता हो दंभ-स्तूप।
श्रद्धा इस संसृति की
रहस्य-व्यापक, विशुद्ध, विश्वासमयी,
सब कुछ देकर नव-निधि अपनी
तुमसे ही तो वह छली गयी।
हो वर्तमान से वंचित तुम
अपने भविष्य में रही रुद्ध
सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध।
तुम जरा मरण में चिर
अशांत
जिसको अब तक समझे थे सब
जीवन में परिवर्तन अनंत,
अमरत्व यही अब भूलूंगा
तुम व्याकुल उसको कहो अंत।
दुखमय चिर चिंतन के
प्रतीक! श्रद्धा-वंचक बनकर अधीर,
मानव-संतति
ग्रह-रश्मि-रज्जु से भाग्य बांध पीटे लकीर।
'कल्याण भूमि यह लोक' यही
श्रद्धा-रहस्य जाने न प्रजा,
अतिचारी मिथ्या मान इसे
परलोक-वंचना से भर जा।
आशाओं में अपने निराश निज
बुद्धि विभव से रहे भ्रांत,
वह चलता रहे सदैव
श्रांत।''
अभिशाप-प्रतिध्वनि हुई लीन
नभ-सागर के अंतस्तल में
जैसे छिप जाता महा मीन,
मृदु मरुत्-लहर में
फेनोपम तारागण झिलमिल हुए दीन।
निस्तब्ध मौन था अखिल लोक
तंद्रालस था वह विजन प्रांत,
रजनी-तम-पुंजीभूत-सदृश
मनु श्वास ले रहे थे अशांत।
वे सोच रहे थे ''आज वही
मेरा अदृष्ट बन फिर आया,
जिसने डाली थी जीवन पर
पहले अपनी काली छाया।
लिख दिया आज उसने भविष्य!
यातना चलेगी अंतहीन,
अब तो अवशिष्ट उपाय भी
न।''
|
|||||


 i
i