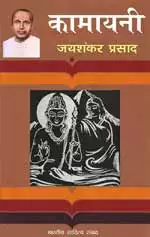|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
''प्रजा तुम्हारी,
तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूं मैं,
वह संदेह-भरा फिर कैसा
नया प्रश्न सुनती हूं मैं!''
''प्रजा नहीं, तुम मेरी
रानी मुझे न अब भ्रम में डालो,
मधुर मराली! कहो 'प्रणय
के मोती अब चुनती हूं मैं'
मेरा भाग्य-गगन
धुंधला-सा, प्राची-पट-सी तुम उसमें,
खुल कर स्वयं अचानक कितनी
प्रभापूर्ण हो छति-यश में!
मैं अतृप्त आलोक-भिखारी ओ
प्रकाश-बालिके! बता,
कब डूबेगी प्यास हमारी इन
मधु-अधरों के रस में?
''ये सुख-साधन और
रुपहली-रातों की शीतल-छाया,
स्वर-संचरित दिशायें, मन
है उन्मद और शिथिल काया,
तब तुम प्रजा बनो मत
रानी!'' नर-पशु कर हुंकार उठा
उधर फैलती मदिर घटा सी
अंधकार की घन - माया।
आलिंगन! फिर भय क्रंदन!
वसुधा जैसे कांप उठी!
वह अतिचारी, दुर्बल
नारी-परित्राण-पथ नाप उठी?
अंतरिक्ष में हुआ
रुद्र-हुंकार भयानक हलचल थी,
अरे आत्मजा प्रजा! पाप की
परिभाषा बन शाप उठी।
उधर गगन में क्षुब्ध हुई
सब देव-शक्तियां क्रोध-भरी
रुद्र-नयन खुल गया
अचानक-व्याकुल कांप रही नगरी,
अतिचारी था स्वयं
प्रजापति, देव अभी शिव बने रहें!
नहीं, इसी से चढ़ी शिंजिनी
अजगव पर प्रतिशोध भरी।
प्रकृति त्रस्त थी,
भूतनाथ ने नृत्य विकंपित-पद अपना-
उधर उठाया, भूत-सृष्टि सब
होने जाती थी सपना!
आश्रय पाने को अब
व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध,
फिर कुछ होगा, यही समझ कर
वसुधा का थर-थर कंपना।
कांप रहे थे प्रलयमयी
क्रीड़ा से सब आशंकित जंतु,
अपनी-अपनी पड़ी सभी को,
छिन्न स्नेह का कोमल तंतु,
आज कहां वह शासन था जो
रक्षा का था भार लिये,
इड़ा क्रोध लज्जा से भर कर
बाहर निकल चली थी किंतु।
|
|||||


 i
i