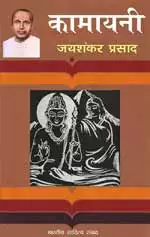|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
यह सारस्वत देश या कि फिर
ध्वंस हुआ सा समझो,
तुम हो अग्नि और यह सभी
धुआं सा?''
''मैंने जो मनु, किया उसे
मत यों कह भूलो,
तुमको जितना मिला उसी में
यों मत फूलो।
प्रकृति संग संघर्ष
सिखाया तुमको मैंने,
तुमको केंद्र बनाकर अनहित
किया न मैंने!
मैंने इस बिखरी-विभूति पर
तुमको स्वामी,
सहज बनाया, तुम अब जिसके
अंतर्यामी।
किंतु आज अपराध हमारा अलग
खड़ा है,
हां में हां न मिलाऊं तो
अपराध बड़ा है।
मनु! देखो यह भ्रांत निशा
अब बीत रही है,
प्राची में नव-उषा तमस्
की जीत रही है।
अभी समय है मुझ पर कुछ
विश्वास करो तो।
बनती है सब बात तनिक तुम
धैर्य धरो तो।''
और एक क्षण वह, प्रसाद का
फिर से आया,
इधर इड़ा ने द्वार ओर निज
पैर बढ़ाया।
किंतु रोक ली गयी भुजाओं
से मनु की वह,
निस्सहाय हो दीन-दृष्टि
देखती रही वह।
''यह सारस्वत देश
तुम्हारा तुम हो रानी।
मुझको अपना अस्त्र बना
करती मनमानी।
|
|||||


 i
i