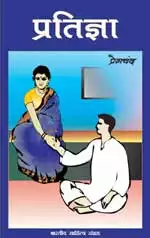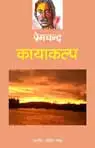|
उपन्यास >> प्रतिज्ञा (उपन्यास) प्रतिज्ञा (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
262 पाठक हैं |
||||||||
‘प्रतिज्ञा’ उपन्यास विषम परिस्थितियों में घुट-घुटकर जी रही भारतीय नारी की विवशताओं और नियति का सजीव चित्रण है
मंगल-सूत्र
ज्ञातव्य
‘मंगल-सूत्र’ प्रेमचंद की अंतिम और अपूर्ण रचना है जिसे वे पूर्ण न कर सके जब विधाता ने उन्हें बुला लिया। इसका बहुत थोड़ा अंश ही वे लिख पाए थे। यह ‘गोदान’ के तुरंत बाद की कृति है जिसमें लेखक अपनी शक्तियों के चरमोत्कर्ष पर था। निस्संदेह यह रचना बहुत महान होती जैसी की प्रारंभिक पृष्ठों से ही पता चल जाता है। लेखक इस उपन्यास को अपने जीवन दर्शन का प्रतीक मान कर चला था। उनका कहना था कि इसकी संपूर्ण परिकल्पना उनके अपने जीवन पर आधारित थी–किन्हीं अर्थों में आप इसे एक आत्मकथात्मक उपन्यास मान सकते हैं। उन्होंने बताया था कि इस कृति के द्वारा वे प्रमाणित करेंगे कि आदर्शों पर चल कर भी कही जाने वाली भौतिक सफलता प्राप्त की जा सकती है–या कम से कम उसका आत्म-संतोष उपलब्ध किया जा सकता है जो अंततोगत्वा जीवन की एकमात्र सार्थकता है। सफलता की प्राप्ति के लिए जीवन में असत्य, नैतिक पतन और नृशंस मानवहीनता तनिक भी अनिवार्य नहीं है। और यह कि जिस सामान्य जीवन को जनसमूह निरादर और तिरस्कार की दृष्टि से देखता है असल में वही उद्दात, सार्थक और स्पृहणीय है। इस नैतिक और दार्शनिक सत्य के स्थापन को प्रेमचंद ने इस उपन्यास रचना का आधार बनाया। लेखक का अपना जीवन इस सत्य का सबसे प्रबल प्रमाण था और उन्होंने इस जीवन द्वारा यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि साहित्यकार एक आदर्श होता है और उसका अस्तित्व देश-काल से निरपेक्ष। मानवता के लिए वह प्रकाशपुंज है जिसका आलोक कभी धूमिल नहीं होता।
१
बड़े बेटे संतकुमार को वकील बना कर, छोटे बेटे साधुकुमार को बी. ए. की डिग्री दिला कर और छोटी लड़की पंकजा के विवाह के लिए स्त्री के हाथों में पाँच हजार रुपये नकद रख कर देवकुमार ने समझ लिया कि वह जीवन के कर्तव्य से मुक्त हो गए और जीवन में जो कुछ शेष रहा है, उसे ईश्वर चिन्तन को अर्पण कर सकते हैं। आज चाहे कोई उन पर अपनी जायदाद को भोगविलास में उड़ा देने का इलजाम लगाए, चाहे साहित्य के अनुष्ठान में, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी आत्मा विशाल थी। यह असंभव था कि कोई उनसे मदद मांगे और निराश हो। भोग विलास जवानी का नशा था और जीवन भर वह उस क्षति की पूर्ति करते रहे, लेकिन साहित्य सेवा के सिवा उन्हें और किसी काम में रुचि न हुई और यहां धन कहां?’–हां यश मिला और उनके आत्मसंतोष के लिए इतना काफी था। संचय में उनका विश्वास भी न था। संभव है, परिस्थिति ने इस विश्वास को दृढ़ किया हो, लेकिन उन्हें कभी संचय न कर सकने का दुःख नहीं हुआ। सम्मान के साथ अपना निर्वाह होता जाए इससे ज्यादा वह और कुछ न चाहते थे। साहित्य-रसिकों में जो एक अकड़ होती है, चाहे उसे शेखी ही क्यों न कर लो, वह उनमें भी थी। कितने ही रईस और राजे इच्छुक थे वह उनके दरबार में जाएं, अपनी रचनाएं सुनाएं उनको भेंट करें, लेकिन देवकुमार ने आत्म-सम्मान को कभी हाथ से न जाने दिया। किसी ने बुलाया भी तो धन्यवाद देकर टाल गए। इतना ही नहीं, वह यह भी चाहते थे कि राजे और रईस मेरे द्वार पर आये, मेरी खुशामद करें, जो अनहोनी बात थी। अपने कई मंदबुद्धि सहपाठियों को वकालत या दूसरे सींगों में धन के ढेर लगाते, जायदादें खरीदते, नए-नए मकान बनवाते देखकर कभी-कभी उन्हें अपनी दशा पर खेद होता था, विशेषकर जब उनकी जन्मसंगिनी शैव्या गृहस्थी की चिन्ताओं से जल कर उन्हें कटु वचन सुनाने लगती थी, पर अपनी रचना-कुटीर में कलम हाथ में लेकर बैठते ही वह सब कुछ भूल साहित्य-स्वर्ग में पहुंच जाते थे। आत्म गौरव जाग उठता था। सारा अवसाद और विषाद शांत हो जाता था।
|
|||||


 i
i