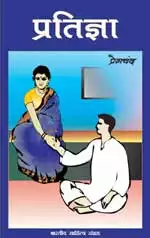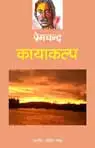|
उपन्यास >> प्रतिज्ञा (उपन्यास) प्रतिज्ञा (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
262 पाठक हैं |
||||||||
‘प्रतिज्ञा’ उपन्यास विषम परिस्थितियों में घुट-घुटकर जी रही भारतीय नारी की विवशताओं और नियति का सजीव चित्रण है
पं. देवकुमार को धमकियों से झुकाना तो असम्भव था मगर तर्क के सामने गर्दन आप ही आप झुक जाती थी। इन दिनों वह यही पहेली सोचते रहते थे कि संसार की कुव्यवस्था क्यों है? कर्म और संस्कार लेकर वह कहीं न पहुंच पाते थे। सर्वात्मवाद से भी उनकी गुत्थी न सुलझती थी। अगर सारा विश्व एकात्म है तो फिर यह भेद क्यों है? क्यों एक आदमी जिंदगी भर बड़ी से बड़ी मेहनत करके भी भूखों मरता है और दूसरा आदमी हाथ पांव न मिलाने पर भी फूलों की सेज पर सोता है। यह सर्वात्म है या घोर अनात्म? बुद्धि जवाब देती–यहां सभी स्वाधीन हैं, सभी को अपनी शक्ति और साधना के हिसाब से उन्नति करने का अवसर है। मगर शंका पूछती–सब को समान अवसर कहां है? बाजार लगा हुआ है। जो चाहे वहां से अपनी इच्छा की चीज खरीद सकता है। मगर खरीदेगा तो वही जिसके पास पैसे हैं। और जब सबके पास पैसे नहीं हैं तो सबका बराबर अधिकार कैसे माना जाए? इस तरह का आत्ममंथन उनके जीवन में कभी न हुआ था। उनकी साहित्यिक बुद्धि ऐसी व्यवस्था से संतुष्ट तो हो ही न सकती थी, पर उनके सामने ऐसी कोई गुत्थी न पड़ी थी जो इस प्रश्न को वैयक्तिक अंत तक ले जाती। इस वक्त उनकी दशा उस आदमी की थी जो रोज मार्ग में ईंटें पड़ी देखता है और बचा कर निकल जाता है। रात में कितने लोगों को ठोकर लगती होगी, कितनों के हाथ-पैर टूटते होंगे, इनका ध्यान उसे नहीं आता। मगर एक दिन जब वह खुद रात-को ठोकर खाकर अपने घुटने फोड़ लेता है तो उसकी निवारण-शक्ति हठ करने लगती है और उस सारे ढेर को मार्ग से हटाने पर तैयार हो जाता है। देवकुमार को वही ठोकर लगी थी! कहां है न्याय? कहां? एक गरीब आदमी किसी खेत में बालें नोच कर खा लेता है, कानून उसे सजा दे देता है। दूसरा अमीर आदमी दिन-दहाड़े दूसरों को लूटता है और उसे पदवी मिलती है, सम्मान मिलता है। कुछ आदमी तरह-तरह के हथियार बांध कर आते हैं और निरीह, दुर्बल मजदूरों पर आतंक जमा कर अपना गुलाम बना लेते हैं। लगान और टैक्स और महसूल और कितने ही नामों में से उसे लूटना शुरू करते हैं, और आप लम्बा-लम्बा वेतन उड़ाते हैं, शिकार खेलते हैं, नाचते हैं, रंग-रलियां मनाते हैं। यही है ईश्वर का रचा हुआ संसार? यही न्याय है?
हां देवता हमेशा रहेंगे और हमेशा रहे हैं। उन्हें अब भी संसार धर्म और नीति पर चलता हुआ नजर आता है। वे अपने जीवन की आहुति देकर संसार से बिदा हो जाते हैं। लेकिन उन्हें देवता क्यों कहो, कायर कहो, आत्मसेवी कहो। देवता वह है जो न्याय की रक्षा करें और उसके लिए प्राण दे दें। अगर वह जान कर अनजन बनता हो तो धर्म से गिरता है और उसकी आंखों में यह कुव्यवस्था खटकती ही नहीं तो वह अन्धा भी है और मूर्ख भी, देवता किसी तरह नहीं। और हां, देवता बनने की जरूरत भी नहीं। देवतओं ने ही भाग्य, ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएँ फैला कर इस अनीति को अमर बनाया है। मनुष्य ने अब तक इस का अन्त कर दिया होता या समाज का ही अन्त कर दिया होता जो इस दशा में जिंदा रहने से कहीं अच्छा होता। नहीं, मनुष्यों को मनुष्य बनना पड़ेगा।!
दरिंदों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं, जड़ता है। आज जो इतने ताल्लुकदार और राजे हैं वह अपने पूर्वजों की लूट का ही आनन्द उठा रहे हैं। और क्या उन्होंने वह जायदाद बेच कर पागलपन नहीं किया? पितरों का पिंड देने के लिए गया जा कर पिंड देना और यहां आकर हजारों रुपयों खर्च करना क्या जरूरी था? और रातों को मित्रों के साथ मुजरे सुनना, और नाटक-मंडली खोल कर हजारों रुपये उसमें डुबाना अनिवार्य था? वह अवश्य पागलपन था। उन्हें क्यों अपने बाल-बच्चों की चिंता नहीं हुई? अगर तुम्हें मुप्त की संपत्ति मिली और उन्होंने उड़ाया तो उनके लड़के क्यों न मुफ्त की संपत्ति भोगें? अगर वह जवानी की उमंगों को नहीं रोक सके तो उनके लड़के क्यों तपस्या करें?
|
|||||


 i
i