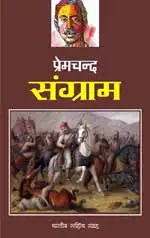|
नाटक-एकाँकी >> संग्राम (नाटक) संग्राम (नाटक)प्रेमचन्द
|
269 पाठक हैं |
||||||||
मुंशी प्रेमचन्द्र द्वारा आज की सामाजिक कुरीतियों पर एक करारी चोट
राजेश्वरी– इसका तो मुझे भी क्या भय है, क्योंकि मैंने सुना है, ज्ञानी देवी उनके बिना एक छन भी नहीं रह सकती। पर मैं भी तो आपके भैया ही के हुक्म की चेरी हूं, जो कुछ वह कहेंगे उसे मानना पड़ेगा। मैं अपना देश, कुल, घर-बार छोड़कर केवल उनके प्रेम के सहारे यहां आयी हूं। मेरा यहाँ कौन है? उस प्रेम सुख उठाने से मैं अपने को कैसे रोकूं? यह तो ऐसा ही होगा कि कोई भोजन बनाकर भूखों तड़पा करे, घरछा कर घूप से जलता रहे। मैं ज्ञानीदेवी से डाह नहीं करती, इतनी ओछी नहीं हूँ कि उनसे बराबरी करूं। लेकिन मैंने जो यह लोक-लज्जा कुल मरजाद तजा है वह किस लिए?
कंचन– इसका मेरे पास क्या जवाब है?
राजेश्वरी– जवाब क्यों नहीं है, पर आप देना नहीं चाहते।
कंचन– दोनों एक ही बात है, भय केवल आपके नाराज होने का है।
राजेश्वरी– इससे आप निंश्चित रहिए; जो प्रेम की आंच सह सकता है, उसके लिए और सभी बातें सहज हो जाती है।
कंचन– मैं इसके सिवा और कुछ न कहूँगा कि आप यहाँ से न जायें।
राजेश्वरी– (कंचन की ओर तिरछी चितवनों से ताकते हुए) यह आपकी इच्छा है?
कंचन– हाँ, यह मेरी प्रार्थना है। (मन में) दिल नहीं मानता, कहीं मुँह से कोई बात निकल न पड़े।
राजेश्वरी– चाहे वह रूठ ही जायें?
कंचन– नहीं, अपने कौशल से उन्हें राजी कर लो।
राजेश्वरी– (मुस्करा कर) मुझमें यह गुण नहीं है।
कंचन– रमणियों में यह गुण बिल्ली के नखों की भाँति छिपा रहता है। जब चाहे उसे काम में ला सकती हैं।
राजेश्वरी– उनसे आपके आने की चर्चा तो करनी ही होगी।
कंचन– नहीं हरगिज नहीं। मैं तुम्हें ईश्वर की कसम दिलाता हूँ। भूलकर भी उनसे यह जिक्र न करना, नहीं तो मैं जहर खा लूँगा, फिर तुम्हें मुँह न दिखाऊँगा।
|
|||||


 i
i