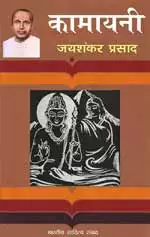|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
लहरें व्योम चूमती उठतीं,
चपलायें असंख्य नचती,
गरल जलद की खड़ी झड़ी में
बूंदे निज संसृति रचती।
चपलायें उस जलधि-विश्व
में स्वयं चमत्कृत होती थीं
ज्यों विराट
बाडव-ज्वालायें खंड-खंड हो रोती थीं।
जलनिधि के तलवासी जलचर
विकल निकलते उतराते,
हुआ विलोड़ित गृह, तब
प्राणी कौन! कहॉ! कब! सुख पाते?
घनीभूत हो उठे पवन, फिर
श्वासों की गति होती रुद्ध,
और चेतना थी विलखाती,
दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध।
उस विराट् आलोड़न में
ग्रह, तारा बुद-बुद से लगते,
प्रखर प्रलय-पावस में
जगमग, ज्योतिरिंगणो-से जगते।
प्रहर दिवस कितने बीते,
अब इसका कौन बता सकता,
इनके सूचक उपकरणों को
चिह्न न कोई पा सकता।
काला शासन-चक्र मृत्यु का
कब तब चला, न स्मरण रहा,
महामत्स्य का एक चपेटा
दीन पोत का मरण रहा।
किंतु, उसी ने ला टकराया
इस उत्तरगिरि के शिर से
देव-सृष्टि का ध्वंस
अचानक श्वास लगा लेने फिर से।
आज अमरता का जीवित हूं
मैं वह भीषण जर्जर दंभ,
आह सर्ग के प्रथम अंक का
अधम-पात्र मय सा विष्कंभ।''
''ओ जीवन की सरु-मरीचिका,
कायरता के अलस विषाद!
अरे पुरातन अमृत! अगतिमय
मोहमुग्ध जर्जर अवसाद!
|
|||||


 i
i