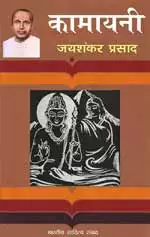|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
इड़ा चकित, श्रद्धा आ बैठी
वह थी मन को सहलाती,
अनुलेपन-सा मधुर स्पर्श
था व्यथा भला क्यों रह जाती?
उस मूर्च्छित नीरवता में
कुछ हल्के से स्पंदन आये,
आंख खुलीं चार कोनों में
चार बिंदु आकर छाये।
उधर कुमार देखता ऊंचे
मंदिर, मंडप, वेदी को,
यह सब क्या है, नया मनोहर
कैसे ये लगते जी को?
मां ने कहा 'अरे आ तू भी
देख पिता हैं पड़े हुए'
'पिता! आ गया लो' यह कहते
उसके रोयें खड़े हुए।
''मां जल दे, कुछ प्यास
होंगे क्या बैठी कर रही यहां?''
मुखर हो गया सूना मंडप यह
सजीवता रही कहां?
आत्मीयता घुली उस घर में
छोटा सा परिवार बना,
छाया एक मधुर स्वर उस पर
श्रद्धा का संगीत बना।
''तुमुल कोलाहल कलह में
मैं हृदय की बात रे मन!
विकल होकर नित्य चंचल
खोजती जब नींद के पल
चेतना थक सी रही तब
मैं वलय की बात रे मन!
चिर-विषाद-विलीन मन की
इस व्यथा के तिमिर वन की;
मैं उषा-सी ज्योति-रेखा
कुसुम-विकसित प्रात रे मन!
|
|||||


 i
i