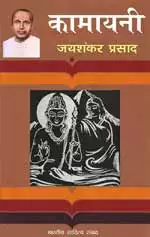|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
सरिता का वह एकांत कूल,
था पवल हिंडोले रहा झूल,
धीरे-धीरे लहरों का दल,
तट से टकरा होता ओझल,
छप छप का होता शब्द विरल,
थर-थर कंप रहती दीप्ति
तरल,
संसृति अपने में रही भूल
वह गंध-विधुर अम्लान फूल।
तब सरस्वती-सा फेंक सांस,
श्रद्धा ने देखा आस-पास,
थे चमक रहे दो खुले नयन,
ज्यों शिलालग्न अनगढ़े
रतन,
वह क्या तम में करता
सनसन?
धारा का ही क्या यह
निस्वन!
ना, गुहा लतावृत एक पास,
कोई जीवित ले रहा सांस!
वह निर्जन तट था एक चित्र,
कितना सुंदर, कितना
पवित्र?
कुछ उन्नत थे वे शैलशिखर,
फिर भी ऊंचा श्रद्धा का
सिर,
वह लोक-अग्नि में तप गल
कर,
थी ढली स्वर्ण-प्रतिमा बन
कर,
मनु ने देखा कितना
विचित्र!
वह मातृ-मूर्ति थी
विश्व-मित्र।
बोले.'रमणी तुम नहीं आह!
जिसके मन में हो भरी चाह,
तुमने अपना सब कुछ खोकर,
वंचिते! जिसे पाया रोकर,
मैं भगा प्राण जिनसे
लेकर,
उसको भी, उन सबको देकर,
निर्दय मन क्या न उठा
कराह?
अद्भुत है तब मन का
प्रवाह!
|
|||||


 i
i