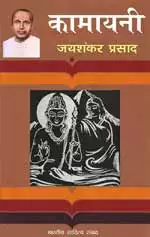|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
92 पाठक हैं |
||||||||
मैं इस निर्जन तट में
अधीर,
सह भूखा व्यथा तीखा समीर,
हां भावचक्र में पिस पिस
कर,
चलता ही आया हूं बढ़ कर,
इनके विकार सा ही बन कर,
मैं शून्य बना सत्ता
खोकर,
लघुता मत देखो वक्ष चीर,
जिसमें अनुशय बन घुसा
तीर।''
''प्रियतम! यह नत
निस्तब्ध रात,
है स्मरण कराती विगत बात,
वह प्रलय शांति वह
कोलाहल,
जब अर्पित कर जीवन संबल,
मैं हुई तुम्हारी थी
निश्छल,
क्या भूलूं मैं, इतनी
दुर्बल?
तब चलो जहां पर शांति
प्रात,
मैं नित्य तुम्हारी, सत्य
बात।
इस देव-द्वंद्व का वह
प्रतीक-
मानव! कर ले सब भूल ठीक,
यह विष जो फैला महा-विषम,
निज कर्मोन्नति से करते
सम,
सब मुक्त बनें, काटेंगे
भ्रम,
उनका रहस्य हो शुभ-संयम,
गिर जायेगा जो है अलीक,
चल कर मिटती है बड़ी लीक।''
वह शून्य असत या अंधकार,
अवकाश पटल का वार पार,
बाहर भीतर उन्मुक्त सघन,
था अचल महा नीला अंजन,
भूमिका बनी वह स्निग्ध
मलिन,
थे निर्निमेष मनु के लोचन,
इतना अनंत था शून्य-सार,
दीखता न जिसके परे पार।
|
|||||


 i
i